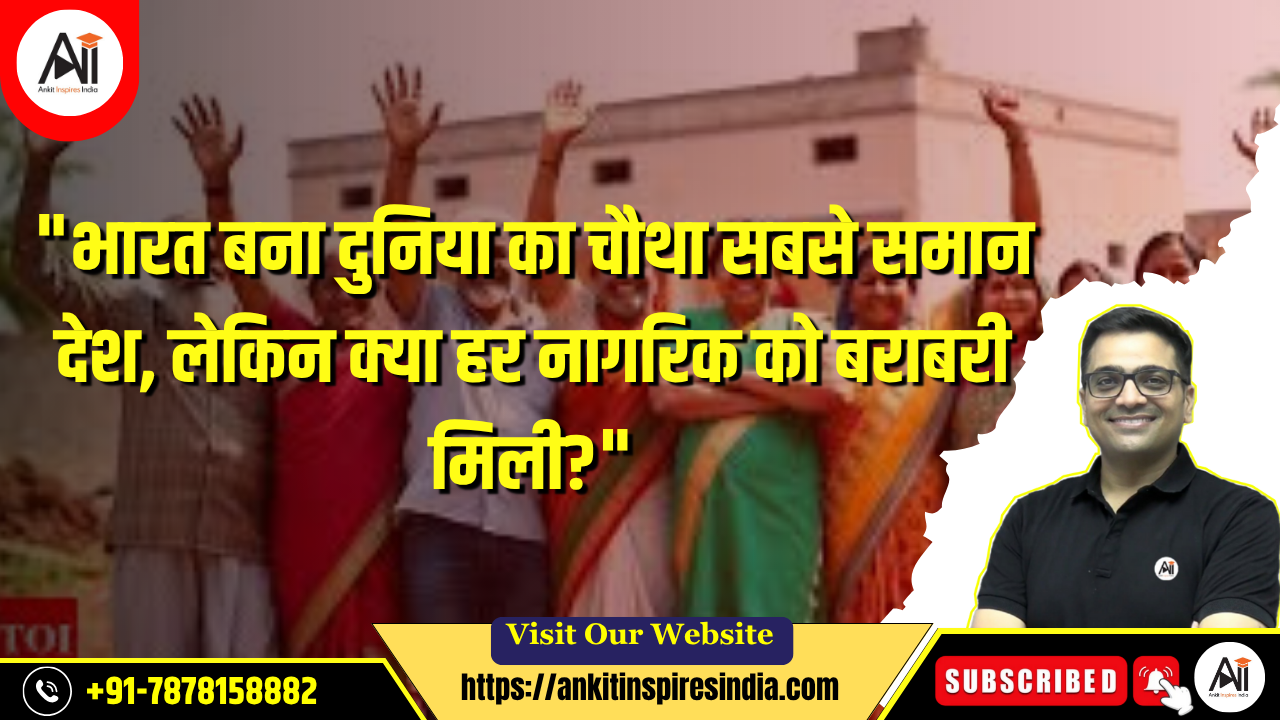भारत ने वैश्विक स्तर पर आय समानता (income equality) के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत आय समानता में दुनिया का चौथा सबसे समान देश बनकर उभरा है। इस सूची में भारत से आगे केवल स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस हैं। यह रैंकिंग दर्शाती है कि भारत अब दुनिया के सबसे अधिक आर्थिक रूप से समान समाजों में शामिल हो चुका है।
भारत का Gini Index स्कोर 25.5 है, जो उसे “मॉडरेटली लो इनइक्वलिटी” (moderately low inequality) श्रेणी में रखता है। यह स्कोर 25 से 30 के बीच के देशों के लिए निर्धारित किया गया है। भारत अब “लो इनइक्वलिटी” (low inequality) वर्ग में आने के बेहद करीब है — उस श्रेणी में वे देश आते हैं जिनका Gini स्कोर 25 से कम है, जैसे स्लोवाक रिपब्लिक (24.1), स्लोवेनिया (24.3) और बेलारूस (24.4)।
भारत का स्कोर चीन (35.7) और अमेरिका (41.8) जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। इतना ही नहीं, भारत इस मामले में हर G7 और G20 देश से अधिक समानता वाला देश बन चुका है, जिनमें से कई को उन्नत अर्थव्यवस्थाएं माना जाता है। यह संकेत देता है कि भारत में आय का वितरण तुलनात्मक रूप से अधिक संतुलित हो रहा है, जो समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

आइए जानते है, Gini Coefficient क्या है?
Gini Coefficient, जिसे Gini Index या Gini Ratio भी कहा जाता है, किसी देश, क्षेत्र या आबादी के भीतर आय या संपत्ति की असमानता को मापने का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। यह सूचकांक यह दर्शाता है कि किसी समाज में आय या धन का वितरण कितना समान या असमान है।
Gini Coefficient का मान 0 से 1 के बीच होता है। यदि किसी देश का Gini स्कोर 0 है, तो इसका अर्थ है कि वहां पूर्ण समानता है — यानी सभी व्यक्तियों की आय या संपत्ति समान है। वहीं, यदि स्कोर 1 है, तो यह दर्शाता है कि वहां पूर्ण असमानता है — यानी एक व्यक्ति के पास सारी संपत्ति है और बाकी सभी के पास कुछ भी नहीं है।
इस सूचकांक की गणना आमतौर पर लोगों या परिवारों की आय या संपत्ति को न्यूनतम से अधिकतम के क्रम में सजाकर की जाती है। फिर एक Lorenz Curve तैयार की जाती है, जो वास्तविक आय वितरण को दर्शाने वाला एक ग्राफ होता है। इस वक्र में जनसंख्या के कुल प्रतिशत की तुलना उनकी कुल आय या संपत्ति के प्रतिशत से की जाती है।
Gini Coefficient की गणना Lorenz Curve और पूर्ण समानता की रेखा (Line of Perfect Equality) के बीच बने क्षेत्रफल को मापकर की जाती है। यह क्षेत्रफल, जो असमानता को दर्शाता है, को पूर्ण समानता के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल से विभाजित कर दिया जाता है। प्राप्त अनुपात ही Gini Coefficient कहलाता है।
इस प्रकार, Gini Coefficient एक सटीक सांख्यिकीय उपकरण है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी देश में आर्थिक संसाधनों का वितरण कितना संतुलित या असंतुलित है।
भारत में बढ़ती आर्थिक समानता – इसका क्या मतलब है ?
भारत में आय समानता के संकेतक के रूप में Gini Coefficient का 25.5 पर होना यह दर्शाता है कि देश में अब अधिक लोग आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में आ रहे हैं। यह परिवर्तन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर व्यापक बदलाव को दर्शाता है। पहले की तुलना में अब अधिक परिवारों को भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकिंग सुविधा और रोज़गार के अवसर सहज रूप से उपलब्ध हो रहे हैं।
यह डेटा इस ओर संकेत करता है कि भारत की आर्थिक प्रगति का लाभ केवल उच्च वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। भारत का यह विकास मॉडल यह साबित करता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक बराबरी एक साथ चल सकते हैं।
यह उदाहरण वैश्विक स्तर पर एक नई दिशा प्रदान करता है, जिसमें विकासशील देश यह दिखा सकते हैं कि समावेशी विकास (inclusive growth) केवल नीतियों का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक हकीकत बन सकता है। इस प्रकार, भारत का यह मार्गदर्शन भविष्य में कई देशों के लिए एक प्रेरणादायी मिसाल बन सकता है।
भारत में आय समानता की दिशा में सुधार – सरकारी योजनाओं की भूमिका
भारत ने आय समानता के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय प्रगति की है, उसके पीछे कई सरकारी योजनाएं और नीतियां रही हैं, जिन्होंने समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ने न केवल गरीबी कम की, बल्कि आर्थिक अवसरों को समान रूप से वितरित करने में भी मदद की है।
सबसे पहले, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिससे करोड़ों गरीब परिवारों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। इससे वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को नई गति मिली।
आधार जैसी योजना ने 142 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल पहचान उपलब्ध करवाई, जिससे सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुंचने लगी। इस पारदर्शिता से लगभग 3.48 लाख करोड़ रुपये की बचत भी हुई, जो पहले लीकेज और बिचौलियों में चली जाती थी।
आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 41 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिला, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी वर्गों की पहुंच सुनिश्चित हुई।
PMGKAY (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई है और गरीबों के लिए जीवन यापन सरल हुआ है।
इसके साथ ही, स्टैंड-अप इंडिया और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय के लिए लोन, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है।
इन योजनाओं के प्रभावशाली कार्यान्वयन का परिणाम यह हुआ कि 2011 से 2023 के बीच लगभग 17.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। इसी अवधि में देश की गरीबी दर 16.2% से घटकर केवल 2.3% रह गई, जो भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति का मजबूत संकेत है।
इस तरह, सरकार की समर्पित नीतियों और योजनाओं ने भारत को आय समानता के क्षेत्र में एक वैश्विक उदाहरण बनने में निर्णायक भूमिका निभाई है।
भारत में गरीबी और बेरोजगारी के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति
भारत ने बीते दशक में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। वर्ल्ड बैंक की नवीनतम रिपोर्ट ‘Poverty and Equity Brief’ के अनुसार, भारत ने 2011-12 से 2022-23 के बीच 171 मिलियन (17.1 करोड़) लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने में सफलता पाई है। इस अवधि में अत्यधिक गरीबी की दर 16.2% से घटकर केवल 2.3% रह गई है, जो भारत की सामाजिक-आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता का प्रमाण है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में गरीबी दर में गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% रह गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 10.7% से घटकर 1.1% हो गई है। इससे ग्रामीण और शहरी गरीबी के बीच का अंतर 7.7 प्रतिशत अंकों से घटकर मात्र 1.7 प्रतिशत अंक रह गया है, जो समावेशी विकास की दिशा में एक सशक्त संकेत है।
सिर्फ गरीबी ही नहीं, भारत ने रोजगार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किया है। वर्ष 2021-22 से भारत में कामकाजी आयु (15-64 वर्ष) में प्रवेश करने वाले लोगों की तुलना में रोजगार के अवसर और तेजी से बढ़े हैं। विशेषकर महिलाओं की रोजगार दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो सामाजिक परिवर्तन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
रिपोर्ट के अनुसार, शहरी बेरोजगारी दर 2024-25 की पहली तिमाही में घटकर 6.6% हो गई है, जो 2017-18 के बाद का सबसे न्यूनतम स्तर है। इसके अलावा, 2018-19 के बाद पहली बार बड़ी संख्या में पुरुष गांवों से शहरों की ओर रोजगार की तलाश में प्रवास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को खेती-बाड़ी और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में अधिक रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।
लेकिन भारत में धन का केंद्रीकरण – एक बढ़ती चुनौती
जहाँ एक ओर भारत गरीबी उन्मूलन और आय समानता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, वहीं दूसरी ओर धन के असमान वितरण को लेकर चिंता भी लगातार बढ़ रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि “धीरे-धीरे गरीबों की संख्या बढ़ रही है और संपत्ति कुछ अमीर लोगों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है — ऐसा नहीं होना चाहिए।” उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित किया जाना चाहिए, जिससे रोजगार सृजन हो और ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान सुनिश्चित किया जा सके।
गडकरी ने धन के विकेंद्रीकरण (Decentralisation of Wealth) की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि “हम ऐसी आर्थिक व्यवस्था की ओर देख रहे हैं जो रोजगार पैदा करे और समावेशी विकास को गति दे।” उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब विभिन्न रिपोर्टें देश में धन के अत्यधिक केंद्रीकरण की ओर संकेत कर रही हैं।
भारत में 1% सबसे अमीर आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 40.1% हिस्सा:
एक स्वतंत्र शोध समूह द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के अंत तक भारत की सबसे अमीर 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 40.1% हिस्सा था, जो 1961 के बाद से अब तक का सबसे ऊँचा स्तर है। इसी रिपोर्ट के अनुसार, उनकी कुल आय में हिस्सेदारी 22.6% थी, जो 1922 के बाद से सबसे अधिक है। यह स्थिति ब्राज़ील और अमेरिका जैसे देशों से भी अधिक असमानता को दर्शाती है, जबकि भारत को एक उभरती हुई समानतावादी अर्थव्यवस्था माना जाता है।
इससे स्पष्ट होता है कि संपत्ति का केंद्रीकरण, आर्थिक समावेशन के रास्ते में एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। यह परिघटना इस ओर इशारा करती है कि जबकि लाखों लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, वहीं आर्थिक विकास का बड़ा हिस्सा अब भी चुनिंदा धनी वर्गों तक सीमित है।
इस संदर्भ में, सरकार को केवल विकास दर (GDP growth) पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी विकास को प्राथमिकता देनी होगी। जब तक संपत्ति और आय का वितरण अधिक संतुलित नहीं होता, तब तक सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की दिशा में भारत की यात्रा अधूरी मानी जाएगी।
भारत में गरीबी मापने के पैमाने और ज़मीनी हकीकत
भारत ने बीते एक दशक में चरम गरीबी (Extreme Poverty) को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अब भी करोड़ों भारतीय बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विश्व बैंक के अनुसार, आज भी भारत की हर चार में से एक आबादी — यानी 35 करोड़ से अधिक लोग, उस न्यूनतम जीवन स्तर से नीचे रह रहे हैं जिसे “सम्मानजनक जीवन” के लिए आवश्यक माना जाता है। ये लोग अब भले ही परंपरागत “अत्यंत गरीब” श्रेणी में न आते हों, लेकिन उनके पास पोषणयुक्त भोजन, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं की स्पष्ट कमी है।
भले ही भारत में गरीबी के स्तर में गिरावट आई है, लेकिन गरीबी मापने के तरीकों में भी बदलाव हुआ है। 2011 के बाद से घरेलू कल्याण में सुधार के कई प्रमाण सामने आए हैं — जैसे बहुआयामी गरीबी में कमी, सामाजिक हस्तांतरण योजनाओं में वृद्धि और प्रति व्यक्ति GDP में वृद्धि। साथ ही, 2022–23 में किए गए सर्वेक्षण में प्रश्नों के प्रारूप और डेटा संग्रह की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिससे घरेलू व्यय की अधिक सटीक गणना संभव हुई है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, $3 प्रतिदिन (PPP के अनुसार) की वैश्विक गरीबी रेखा के आधार पर अब भारत की केवल 5% आबादी अत्यधिक गरीबी में है, जो 2011 में 27% थी। यानी करीब 26.9 करोड़ लोग एक दशक में अत्यधिक निर्धनता से बाहर निकले हैं।
लेकिन विश्व बैंक के अनुसार, $3 प्रति दिन की सीमा अब भारत के विकास के वर्तमान स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। अब भारत के लिए उपयुक्त मानक $4.20 प्रति दिन (PPP के अनुसार) है, जो लगभग ₹87 प्रतिदिन बनता है (IMF के 2025 के PPP रेट — ₹20.66 प्रति डॉलर — के आधार पर)। इस मानक के अनुसार, भारत की लगभग 23.9% आबादी अब भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है।
निष्कर्ष:
भारत ने बीते दशक में गरीबी उन्मूलन, बहुआयामी विकास, और आय समानता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। करोड़ों लोग चरम निर्धनता से बाहर निकले हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे जनधन, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ने निचले तबके को सहारा दिया है।
लेकिन इन आँकड़ों की चमक के पीछे कुछ अहम नीतिगत और व्यावहारिक चुनौतियाँ भी छिपी हैं। $3 प्रतिदिन जैसी गरीबी रेखा, आज के भारत की वास्तविक जीवन लागत को प्रतिबिंबित नहीं करती। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भले ही “आधिकारिक रूप से गरीब” न हों, लेकिन अब भी पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी ज़रूरतों से वंचित हैं।