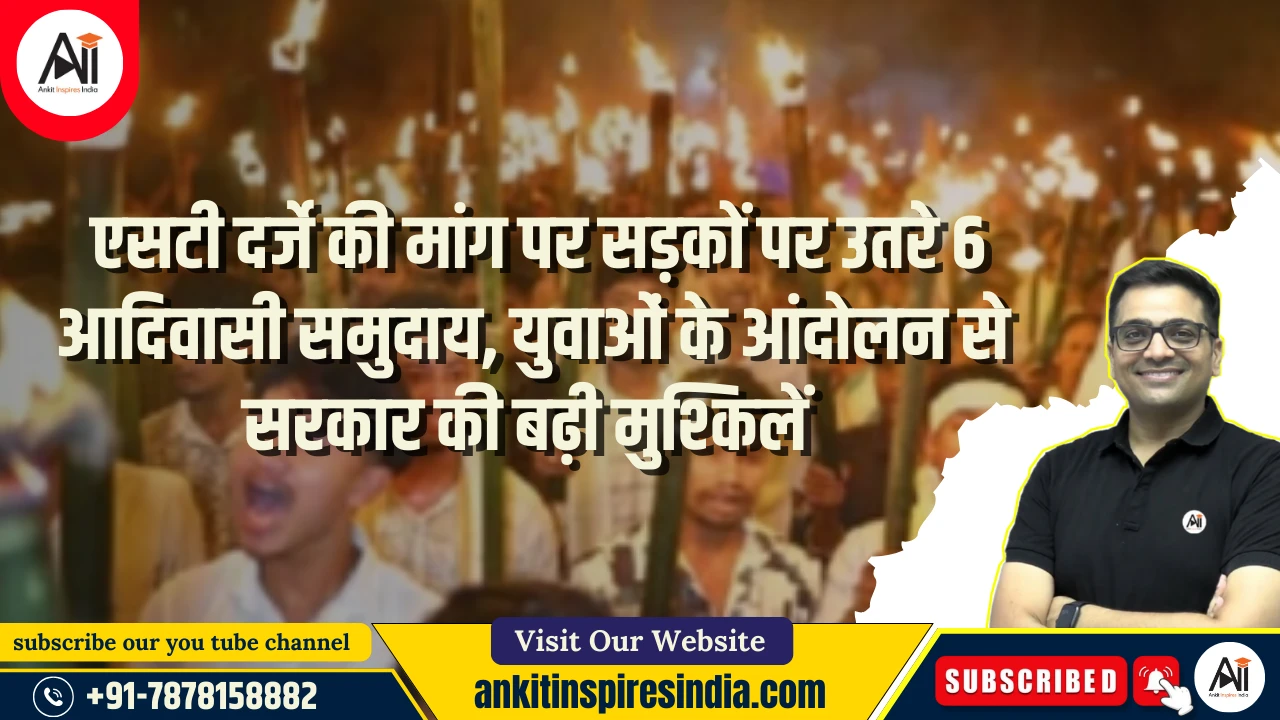असम में इन दिनों मटक समुदाय (Matak Community) सड़कों पर उतर आया है। बीते दस दिनों से उनकी ओर से बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन और मशाल रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जिनमें 30–40 हजार आदिवासी शामिल हुए। डिब्रूगढ़ से लेकर कई जिलों तक 6 आदिवासियों का समूह लगातार रैली कर रहा है। मटक समुदाय की मुख्य मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) का दर्जा और पूर्ण स्वायत्तता (Autonomy) मिले। इसके साथ ही पाँच अन्य जनजातियाँ भी इसी तरह की मांग कर रही हैं।

मटक समुदाय (Matak Community) मांगें क्या है?
मटक समुदाय की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:
- अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा:यह मटक समुदाय की सबसे मुख्य मांग है। वे अपने समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरी और अन्य योजनाओं में आरक्षण का लाभ मिल सके।
- पूर्ण स्वायत्तता:समुदाय अपने विकास और संस्कृति के संरक्षण के लिए स्वायत्तता की मांग भी कर रहा है।
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व:मटक समुदाय अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सरकार में अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहता है।
- आर्थिक विकास:समुदाय के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए आर्थिक सहायता और विकास परियोजनाओं की भी मांग की जाती है।
पिछले कुछ समय से मटक समुदाय और असम के अन्य आदिवासी समुदाय, जैसे ताई-अहोम, मोरन, चुटिया और कोच-राजबोंगशी, इन मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
मटक समुदाय की पुरानी मांग पर बढ़ा तनाव, चुनाव से पहले सरकार के लिए बड़ी चुनौती
बता दें कि मटक समुदाय की यह मांग कोई नई नहीं है, बल्कि काफी पुरानी है। इस मुद्दे पर उनके प्रतिनिधियों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। अब जबकि असम में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर दबाव और तनाव दोनों बढ़ गए हैं। इसी कारण वे बार-बार मटक समुदाय को बातचीत के लिए बुला रहे हैं, मगर समुदाय ने साफ कर दिया है कि वे इस बार सरकार के साथ बातचीत की मेज पर नहीं बैठेंगे।
असम विधानसभा चुनाव 2026 :
असम में अगले विधानसभा चुनाव मार्च से अप्रैल 2026 के बीच कराए जाएंगे। इसमें असम विधानसभा की कुल 126 सीटों के लिए सदस्य चुने जाएंगे।
वर्तमान विधानसभा, जो 2021 में निर्वाचित हुई थी, उसका कार्यकाल 2 मई 2026 को समाप्त होगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने संकेत दिया है कि वे चुनाव तक अपनी भूमिका निभाते रहेंगे।
असम सरकार को क्यों सता रहा है डर?
असम में मटक समुदाय के साथ पाँच अन्य आदिवासी समुदाय भी अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा मांग रहे हैं- चाय जनजाति, ताई अहोम, मोरन, चुटिया और कोच राजबोंगशी। गौरतलब है कि भाजपा सरकार ने 2014 का आम चुनाव जीतने के बाद इन्हें एसटी का दर्जा देने का वादा किया था।
- जनसंख्या का संतुलन बदलने की आशंका: 2011 की जनगणना के अनुसार, असम की कुल आबादी 12 करोड़ थी, जिसमें 38 लाख यानी लगभग 12.4% आदिवासी थे। यदि इन छह समुदायों को एसटी दर्जा मिल जाता है तो यह अनुपात बढ़कर करीब 40% तक पहुँच जाएगा।
- गैर-आदिवासी समुदायों की चिंता: राज्य के गैर-आदिवासियों को डर है कि यदि एसटी आबादी 50% तक पहुँच गई, तो असम भी नगालैंड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तरह एक पूर्ण एसटी राज्य बन जाएगा।
- छठी अनुसूची में शामिल होने का दबाव: ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को मजबूरन असम को छठी अनुसूची में शामिल करना पड़ सकता है। इसका मतलब होगा कि राज्य के प्रशासनिक और विकास संबंधी अधिकांश कार्यों के लिए केंद्र सरकार को स्थानीय जनजातीय निकायों से अनुमति लेनी पड़ेगी।
क्या है मटक समुदाय?
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: मटक समुदाय असम के इतिहास से गहराई से जुड़ा है। 18वीं सदी में जब अहोम साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तब मटक समुदाय एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा।
- संस्कृति और धर्म: मटक समुदाय पर महापुरुषिया संप्रदाय (श्रीमनता शंकरदेव की परंपरा) का गहरा प्रभाव है. वे अपनी विशिष्ट बोली, रीति-रिवाज और सामुदायिक जीवन के लिए पहचाने जाते हैं।
- निवास क्षेत्र: मटक लोगों का मुख्य निवास ऊपरी असम है, खासकर डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों के आसपास।
- मोअमोरिया आंदोलन से पहचान: मटक समुदाय की पहचान मुख्य रूप से मोअमोरिया आंदोलन से होती है। इस आंदोलन में उन्होंने अहोम राजशाही के खिलाफ विद्रोह किया था।
- स्वायत्त क्षेत्र की मान्यता: इस संघर्ष के बाद, 1805 में अहोम राज्य ने मटक को एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में मान्यता दी। यहाँ पर शासन के लिए बारसेनापति (Barsenapati) की उपाधि देकर शासक की नियुक्ति की जाती थी।
- राजनीतिक चेतना: अंग्रेज़ों के आगमन के दौरान और स्वतंत्रता संग्राम में भी मटक युवाओं और नेताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई।
असम के आदिवासियों की चुनौतियाँ:
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी: मटक, मोरान और चाय जनजाति जैसे आदिवासी समुदाय लंबे समय से राजनीतिक रूप से हाशिए पर रहे हैं। वर्तमान में इन्हें ओबीसी (OBC) वर्ग में रखा गया है, जबकि इनकी प्रमुख मांग अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा है।
- भूमि अधिकारों पर संकट: इनका दावा है कि असम में चाय बागानों और आरक्षित वनों के विस्तार के चलते उनकी परंपरागत ज़मीन उनसे छीनी जाती रही है। इस कारण आज भी ये समुदाय भूमि सुरक्षा की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं।
- शिक्षा और रोजगार में पिछड़ापन: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच और सरकारी नौकरियों में अवसरों की कमी ने इन्हें मुख्यधारा से दूर कर दिया है।
- संस्कृति और पहचान पर खतरा: इन आदिवासी समुदायों की भाषा, परंपरा और लोककला धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है।
असम के आदिवासी समूह-
असम अनेक विविध आदिवासी समुदायों का घर है। इन्हें मुख्य रूप से मैदानी जनजातियों और पहाड़ी जनजातियों में बाँटा गया है। इनके अलावा कुछ अन्य विशिष्ट समूह भी हैं जो अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं।
- मैदानी जनजातियाँ:
- बोडो: असम का सबसे बड़ा स्वदेशी समुदाय, मुख्यतः ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्सों में बसे हुए।
- मिशिंग: असम के बड़े समुदायों में से एक, धेमाजी, लखीमपुर, सोनितपुर और गोलाघाट जिलों के नदी किनारे रहने वाले।
- राभा: राज्य की संस्कृति और परंपराओं में अहम योगदान देने वाला समुदाय।
- सोनोवाल कछारी: असम की एक प्रमुख मैदानी जनजाति।
- लालुंग (तिवा): अपनी अनूठी भाषा और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध।
- देवरी: समृद्ध लोक संस्कृति और परंपरा के लिए जानी जाने वाली जनजाति।
- पहाड़ी जनजातियाँ:
- कार्बी: कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ जिलों में निवास करने वाला प्रमुख समुदाय।
- डिमासा: दिमा हसाओ जिले का प्रमुख आदिवासी समूह।
- गारो: असम और मेघालय में पाए जाने वाले समुदाय।
- कुकी: पहाड़ी क्षेत्रों में फैले विभिन्न कुकी समूह।
- अन्य प्रमुख समूह:
- ताई अहोम: ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना करने वाले, आज एसटी दर्जे की माँग कर रहे हैं।
- चाय जनजातियाँ: ब्रिटिश शासन के दौरान चाय बागानों में काम करने के लिए लाए गए, वर्तमान में असम की लगभग 18% आबादी। ये भी एसटी दर्जा पाने की माँग कर रहे हैं।
- मटक, मोरन और कोच राजबोंगशी: ये भी लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की माँग कर रहे हैं।
असम में स्वायत्तता का ढांचा:
असम में पूर्ण स्वायत्तता नहीं है, लेकिन संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) और अनुच्छेद 244(ए) के तहत कुछ जनजातीय क्षेत्रों को सीमित स्वायत्तता दी गई है।
- स्वायत्त जिले और परिषदें:
- छठी अनुसूची असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करती है।
- इसके तहत ज़िला परिषद और क्षेत्रीय परिषदें अपने रीति-रिवाज, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मामलों में नियम और कानून बना सकती हैं।
- ये परिषदें सरकारी धन भी प्राप्त कर सकती हैं, जिससे स्थानीय विकास में योगदान मिलता है।
- अनुच्छेद 244(ए):
- यह अनुच्छेद संसद को असम में कुछ जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त राज्य बनाने का अधिकार देता है। इसे 1969 के 22वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और यह संसद को ऐसे स्वायत्त राज्य को विधानमंडल या मंत्रिपरिषद (या दोनों) के साथ शक्तियां प्रदान करने का अधिकार देता है. यह छठी अनुसूची के तहत आने वाले स्वायत्त परिषदों से भिन्न है, क्योंकि इसमें कानून और व्यवस्था जैसे मामलों पर अधिक स्वायत्तता की परिकल्पना की गई है।
- स्वायत्त राज्य में अलग विधायिका और मंत्रिपरिषद हो सकती है।
- यह प्रावधान कार्बी आंगलोंग जैसे क्षेत्रों में उग्रवादी समूहों के शांति समझौते को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया।
- मांग और वास्तविक स्थिति:
- कई आदिवासी समूह जैसे राभा, कार्बी और डिमासा स्वायत्त राज्य की मांग करते रहे हैं।
- हालाँकि, स्वायत्त परिषदों की वास्तविक स्वायत्तता में कुछ सीमाएँ हैं: चुनावों का अभाव, केंद्र और राज्य सरकार के वित्तपोषण पर निर्भरता
- हाल के वर्षों में कुछ परिषदों को अधिक स्वायत्तता देने या राज्य नियंत्रण बढ़ाने के लिए संशोधन भी किए गए हैं।
निष्कर्ष: जनजातीय समुदायों के वास्तविक विकास के लिए केवल आरक्षण पर्याप्त नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों को ठोस निर्णय लेते हुए यह तय करना होगा कि किन समुदायों को एसटी सूची में शामिल किया जाए। साथ ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आधारभूत सुविधाओं पर समान ध्यान देना होगा। भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए सामुदायिक संग्रहालय, शिक्षा पाठ्यक्रम में जनजातीय सामग्री और सांस्कृतिक अनुदान जैसी पहल अनिवार्य हैं। इस प्रकार ही सामाजिक न्याय और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सकेगा।