ब्राज़ील के बेलें शहर में 10-21 नवम्बर 2025 तक आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP30) से अफगानिस्तान को आमंत्रण न मिलने पर तालिबान सरकार ने गहरा असंतोष व्यक्त किया है। अफगानिस्तान की नेशनल एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (NEPA) ने कहा है कि दुनिया के सबसे जलवायु-संवेदनशील देशों में शामिल होने के बावजूद अफगानिस्तान को इस वैश्विक मंच से बाहर रखना “जलवायु न्याय, वैश्विक सहयोग और मानवीय एकजुटता” के सिद्धांतों के खिलाफ है।
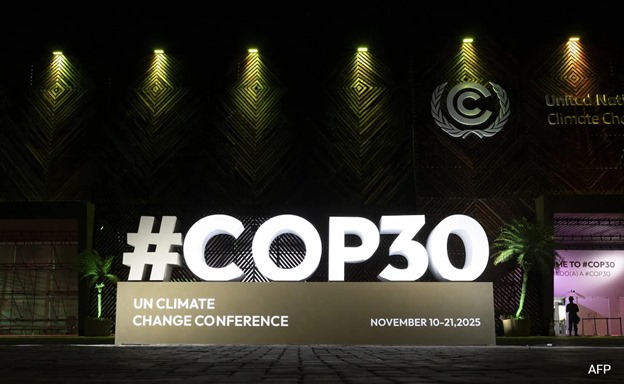
राजनयिक अलगाव, लेकिन पर्यावरण पर सक्रियता
2021 में सत्ता में लौटने के बाद से तालिबान सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीमित मान्यता प्राप्त है – औपचारिक रूप से केवल रूस ने उसे मान्यता दी है। इसके बावजूद तालिबान का कहना है कि राजनयिक अलगाव जलवायु वार्ताओं में भागीदारी की राह में बाधा नहीं बनना चाहिए।
पिछले वर्ष तालिबान प्रतिनिधियों ने अज़रबैजान में आयोजित COP29 में मेज़बान देश के अतिथि के रूप में भाग लिया था, पर वे औपचारिक वार्ताओं का हिस्सा नहीं थे। इस बार, अफगान सरकार ने “Afghanistan on the Road to COP30” नाम से काबुल में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था ताकि वैश्विक जलवायु एजेंडा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके।
कृषि पर निर्भर देश, गंभीर जलवायु संकट से जूझता अफगानिस्तान
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अफगानिस्तान की लगभग 89% आबादी कृषि पर निर्भर है, जिससे यह देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील बन जाता है।
देश में बढ़ते सूखे, घटते भूजल स्तर और बढ़ते तापमान ने लाखों लोगों की आजीविका को खतरे में डाल दिया है।
2020 से 2025 के बीच लगातार आए सूखे ने जलस्तर को कई इलाकों में 30 मीटर तक गिरा दिया, जिससे ग्रामीण समुदायों में मानवीय संकट पैदा हो गया। विशेषज्ञों के मुताबिक, अफगानिस्तान का वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में हिस्सा मात्र 0.06% है, लेकिन इसके बावजूद यह जलवायु प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है।
अंतरराष्ट्रीय बहिष्कार या जलवायु न्याय की चुनौती
COP30 से अफगानिस्तान की अनुपस्थिति ने जलवायु नीति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के बीच के जटिल संबंधों को उजागर किया है। तालिबान को अधिकांश देशों द्वारा मान्यता न मिलने के कारण वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित सम्मेलनों में औपचारिक रूप से भाग नहीं ले सकता।
पर्यावरण विशेषज्ञों का तर्क है कि जलवायु वार्ताओं में सभी प्रभावित देशों और समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए, चाहे उनकी राजनीतिक स्थिति कुछ भी हो, क्योंकि जलवायु संकट सीमाओं और सरकारों से परे है।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) क्या है? UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयासों का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधि (Treaty) है। यह संधि जलवायु परिवर्तन को सीमित करने और इसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करती है। · मुख्य उद्देश्य:
· उत्पत्ति और उद्देश्य: UNFCCC को 1992 में रियो अर्थ समिट (Rio Earth Summit) में अपनाया गया था। यह तीन प्रमुख “रियो कन्वेंशनों” में से एक है — o UN Convention on Biological Diversity (CBD) – जैव विविधता की सुरक्षा के लिए, o UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) – मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए, o UNFCCC – जलवायु परिवर्तन के लिए। · सदस्यता और संरचना o UNFCCC के 198 सदस्य (Parties) हैं — जिनमें 197 देश और यूरोपीय संघ (EU) शामिल हैं। o यह इसे दुनिया की सबसे व्यापक रूप से अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय संधियों में से एक बनाता है। o हर साल सदस्य देश Conference of the Parties (COP) बैठकों में मिलते हैं, जहाँ पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा और नए जलवायु कदम तय किए जाते हैं। वैज्ञानिक आधार: IPCC की भूमिका · UNFCCC के निर्णय IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) की वैज्ञानिक रिपोर्टों पर आधारित होते हैं। · IPCC की स्थापना 1988 में UNEP (United Nations Environment Programme) और WMO (World Meteorological Organization) द्वारा की गई थी। यह संगठन जलवायु परिवर्तन से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी का मूल्यांकन करता है और नीति-निर्माताओं को दिशा प्रदान करता है। क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) – 1997: क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC के अंतर्गत 1997 में अपनाया गया एक कानूनी समझौता है, जिसने विकसित देशों के लिए स्पष्ट उत्सर्जन कटौती लक्ष्य तय किए। मुख्य विशेषताएँ:
पेरिस समझौता (Paris Agreement) – 2015 पेरिस समझौता दिसंबर 2015 में COP21 (पेरिस) में अपनाया गया। मुख्य उद्देश्य: 1. वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे रखना, और इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास करना। 2. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लचीलापन (resilience) और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना। 3. वित्तीय प्रवाह को जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप बनाना। राष्ट्रीय योगदान (Nationally Determined Contributions – NDCs) पेरिस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हर देश को स्वयं अपने जलवायु लक्ष्यों (NDCs) को तय करने की स्वतंत्रता दी गई है।
|
COP30: जलवायु कार्रवाई का ‘Implementation COP’
बेलें (ब्राज़ील) में आयोजित यह सम्मेलन 21 नवंबर तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है-
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए वैश्विक संकल्पों को मजबूत करना।
- विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की नई रूपरेखा बनाना।
- जलवायु न्याय और समानता के सिद्धांतों के तहत जिम्मेदारियों को संतुलित करना।
प्रमुख एजेंडा और पहलें
- Global Stocktake (GST): पेरिस समझौते के बाद पहली व्यापक समीक्षा।
- New Collective Quantified Goal (NCQG): जलवायु वित्त को 2035 तक $300 बिलियन वार्षिक तक बढ़ाने का लक्ष्य।
- Global Goal on Adaptation (GGA): जलवायु अनुकूलन के लिए स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य।
- Tropical Forests Forever Facility (TFFF): उष्णकटिबंधीय वनों की सुरक्षा के लिए ब्राज़ील-नेतृत्व वाली पहल।
प्रमुख वैश्विक घटनाएँ
इस वर्ष की COP30 का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह पेरिस समझौते के 10 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहा है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में पद संभालते ही अमेरिका को पेरिस समझौते से वापस ले लिया। वहीं सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरआ पहली बार इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं – यह 1995 में सम्मेलन की स्थापना के बाद सीरियाई राष्ट्रपति की पहली भागीदारी है।
निष्कर्ष:
अफगानिस्तान की COP30 से अनुपस्थिति केवल एक राजनयिक निर्णय नहीं, बल्कि यह एक वैश्विक नैतिक प्रश्न बन गई है – क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर जलवायु न्याय को प्राथमिकता दे पाएगा? जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता यह साबित कर रही है कि इसका प्रभाव सीमाओं, सरकारों और मान्यता से परे है।



