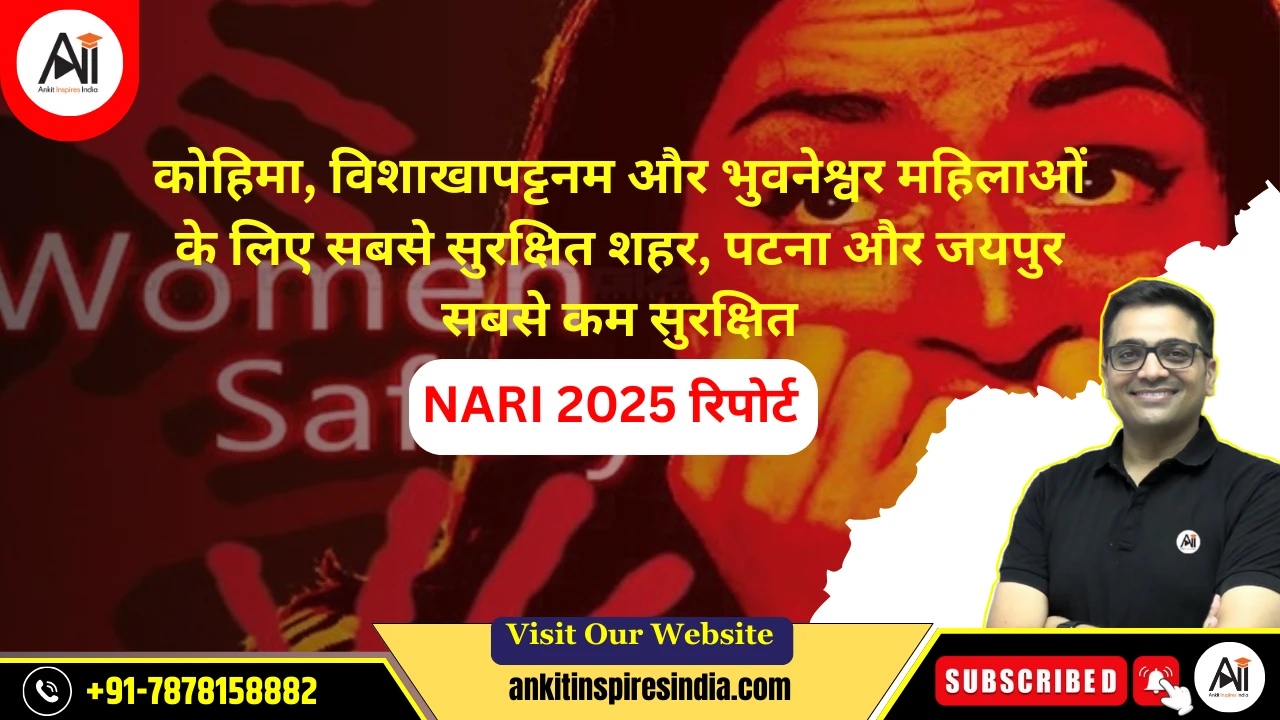राष्ट्रीय महिला आयोग (NMC) ने हाल ही में नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेंस सेफ्टी (NARI) 2025 जारी किया है। इस सर्वे में देश के 31 शहरों की 12,770 महिलाओं की राय ली गई, जिसके आधार पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े अहम आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ शहर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माने गए हैं, जबकि कुछ शहरों को सबसे कम सुरक्षित की श्रेणी में रखा गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, देश के शहरी क्षेत्रों में 40% महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं। कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई को सबसे सुरक्षित शहरों में स्थान दिया गया है, जबकि रांची, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, पटना और जयपुर को सबसे कम सुरक्षित शहरों में गिना गया है।
महिला सुरक्षा पर सर्वेक्षण का निष्कर्ष
- सर्वेक्षण का दायरा: 18 वर्ष से अधिक आयु की 12,770 महिलाओं से राय ली गई।
- महिला सुरक्षा की धारणा: देशभर में औसतन 6% महिलाएं अपने शहर में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। इसका मतलब है कि लगभग 35–36% महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं।
- मापदंड: महिला सुरक्षा का आकलन केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है। इसमें शामिल हैं: संपूर्ण सुरक्षा, पड़ोस और स्थानीय परिवेश, सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा संस्थान, कार्यस्थल, स्वास्थ्य सेवाएँ, मनोरंजन और सार्वजनिक स्थल, ऑनलाइन उत्पीड़न
- संपर्क और शिकायत प्रणाली: यह मापदंड ढांचागत संसाधनों के अलावा उत्पीड़न की घटनाओं और उनकी शिकायतों को भी ध्यान में रखते हैं।
सुरक्षित और असुरक्षित शहरों के पीछे की वजहें:
NARI-2025 रिपोर्ट के अनुसार, कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई जैसे शहर महिलाओं की सुरक्षा रैंकिंग में शीर्ष पर रहे। इन शहरों में अपेक्षाकृत बेहतर पुलिस व्यवस्था, महिला अनुकूल बुनियादी ढांचा, लैंगिक समानता और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को मुख्य कारण माना गया है।
इसके विपरीत, पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची जैसे शहर सूची में सबसे नीचे रहे। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में कमजोर आधारभूत सुविधाएँ, पितृसत्तात्मक सोच और संस्थागत जवाबदेही की कमी को रेखांकित किया गया है।
कुल मिलाकर, सर्वेक्षण में शामिल महिलाओं में से लगभग 60% ने अपने शहर में सुरक्षा की भावना व्यक्त की, जबकि शेष 40% ने खुद को अपेक्षाकृत असुरक्षित बताया।
सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न और सुरक्षा को लेकर महिलाओं की धारणा:
NARI-2025 रिपोर्ट ने यह भी उजागर किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा अब भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार, हर तीन में से दो महिलाओं ने माना कि वे ऐसे मामलों की शिकायत नहीं करतीं। वर्ष 2024 में सर्वेक्षण में शामिल लगभग 7 प्रतिशत महिलाओं ने किसी न किसी रूप में उत्पीड़न का अनुभव किया, जिनमें 18 से 24 वर्ष की युवतियाँ सबसे अधिक प्रभावित रहीं। यह आँकड़ा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के 2022 के 0.07 प्रतिशत के आधिकारिक आंकड़े से कहीं अधिक है, क्योंकि यह रिपोर्ट प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है और इसमें वे मामले भी सामने आते हैं, जो अक्सर दर्ज नहीं हो पाते।
33% ने दर्ज कराई शिकायत, मात्र 16% मामलों में हुई कार्रवाई:
चिंताजनक तथ्य यह है कि उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिलाओं में केवल 33 प्रतिशत ने मामले को रिपोर्ट किया और इनमें से महज 16 प्रतिशत में ही वास्तविक कार्रवाई हुई। सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसे की स्थिति भी कमजोर रही, क्योंकि मात्र 25 प्रतिशत महिलाओं ने ही शासन-प्रशासन की प्रभावी कार्रवाई पर विश्वास जताया। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि रात के समय महिलाओं की असुरक्षा की भावना अधिक बढ़ जाती है, जिसका प्रमुख कारण अधूरी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ जैसे अपर्याप्त स्ट्रीट लाइटिंग, सीमित पुलिस पेट्रोलिंग और सामाजिक रवैया हैं।
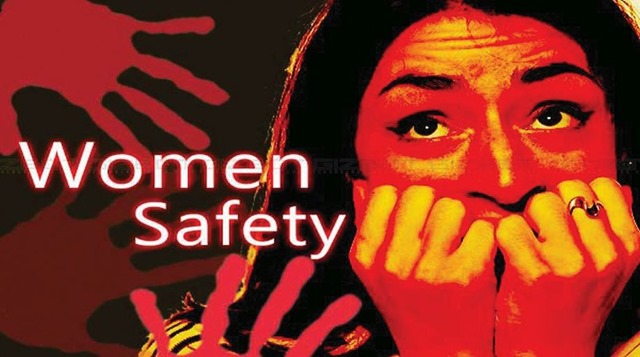
कार्यस्थल सुरक्षित स्थान के रूप में उभर रहे हैं
रिपोर्ट के अनुसार, कार्यस्थल अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थानों के रूप में सामने आए हैं। लगभग 91% महिलाओं ने कहा कि वे कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करती हैं। वहीं, लगभग आधी महिलाओं ने स्वीकार किया कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि उनके संगठन में यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) नीति लागू है या नहीं। इसके अलावा, 69% महिलाओं का मानना है कि वर्तमान सुरक्षा उपाय “कुछ हद तक पर्याप्त” हैं, जबकि 30% से अधिक महिलाओं ने मौजूदा व्यवस्थाओं में कमियों की ओर इशारा किया।
पड़ोस और परिवहन बने उत्पीड़न के मुख्य केंद्र: रिपोर्ट के अनुसार, उत्पीड़न की सबसे अधिक घटनाएं पड़ोस (38%) और परिवहन (29%) में दर्ज की गईं। यह आंकड़े बताते हैं कि कार्यस्थल भले ही अपेक्षाकृत सुरक्षित हों, लेकिन घर से बाहर निकलते ही महिलाओं को असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कानूनी प्रतिक्रिया में चुनौतियाँ:
- अपर्याप्त कानूनी कार्रवाई: हिंसा के मामलों का अक्सर प्रभावी समाधान नहीं होता, जैसा कि कोलकाता के एक मामले में देखा गया।
- कम सजा और दोषसिद्धि दर: दहेज हत्या जैसे गंभीर मामलों में भी दोषसिद्धि कम होती है, क्योंकि अक्सर मामले शांति समझौते में बदल जाते हैं।
- घरेलू हिंसा पर कमजोर कानून: घरेलू हिंसा से जुड़े कानून कम प्रभावी हैं और अपराधियों को न्यूनतम सजा मिलती है।
- सहज जमानत नियम: पीछा करने और उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों में अपराधियों को आसानी से जमानत मिल जाती है।
- धीमा न्यायिक प्रक्रिया: मुकदमे लंबित रहते हैं और कई मामलों को उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना निपटाया जाता है
भारत में महिला सुरक्षा के लिए किए गए उपाय:
भारत सरकार ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम और कानूनी ढांचे लागू किए हैं। इनमें प्रमुख हैं:
- निर्भया फंड (2013): महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पैनिक बटन, सीसीटीवी निगरानी जैसी सुरक्षा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- वन स्टॉप सेंटर (OSC) योजना (2015): हिंसा से प्रभावित महिलाओं को कानूनी, चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी एकीकृत सहायता उपलब्ध कराती है।
- महिला हेल्पलाइन (181): संकट में महिलाओं को 24/7 तत्काल और आपातकालीन सहायता, पुलिस, अस्पताल और वन स्टॉप सेंटर से संपर्क उपलब्ध कराती है।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015): लिंग आधारित भेदभाव को कम करने और बालिकाओं की स्थिति व कल्याण में सुधार लाने के लिए कार्यरत।
- मिशन शक्ति: महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए व्यापक अभियान, जिसमें सुरक्षा (“संबल”) और सशक्तिकरण (“समर्थ्य”) के उप-योजनाएँ शामिल हैं।
- महिला पुलिस स्वयंसेवक (MPV): समाज और पुलिस के बीच पुल का काम करती हैं और जरूरतमंद महिलाओं की सहायता करती हैं।
- उज्जवला योजना: मानव तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार महिलाओं को बचाने, पुनर्वासित करने और समाज में पुनः एकीकृत करने पर केंद्रित।
वैश्विक पहलें महिला सुरक्षा के लिए:
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस: संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 नवंबर को मनाया जाता है।
- UN Women Safe Cities Initiative: महिलाओं और लड़कियों के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाने का प्रयास।
- Gender Inclusive Cities Programme: यूएन ट्रस्ट फंड द्वारा वित्त पोषित, यह शहरों में महिलाओं की सुरक्षा सुधारने के लिए काम करता है।
- UN Development Fund for Women (UNIFEM): लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्थन प्रदान करता है।