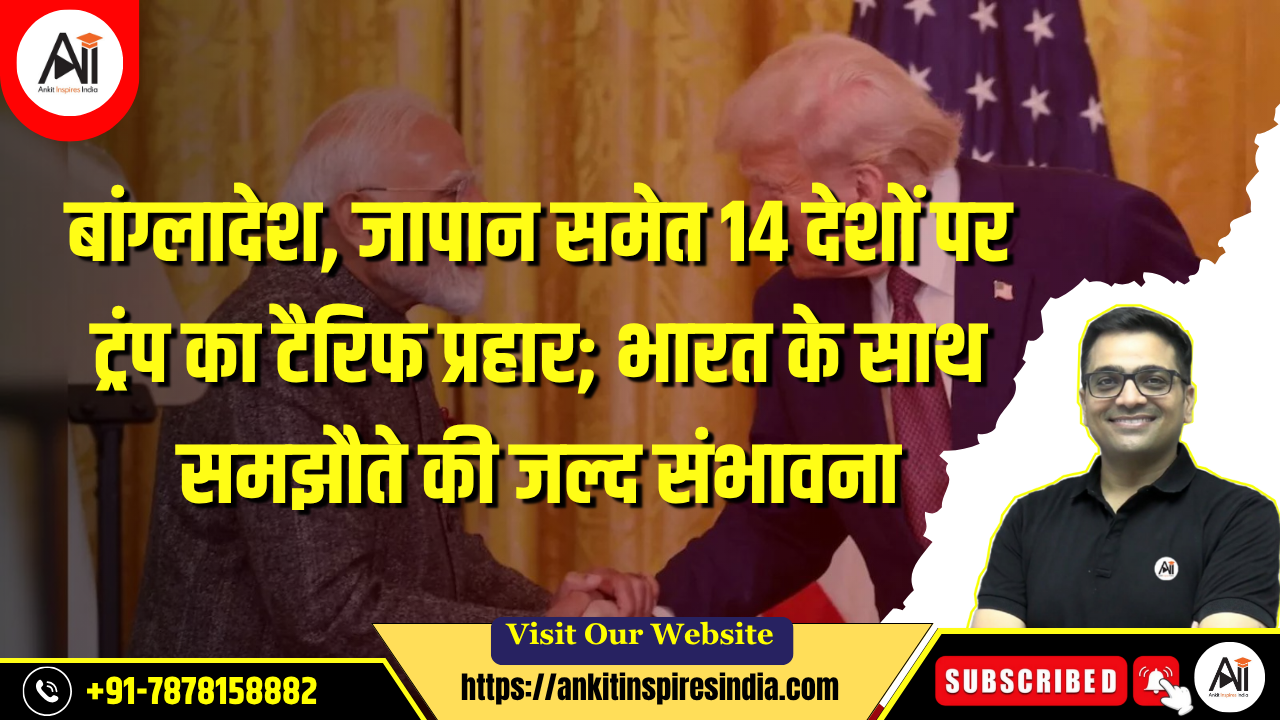अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति एक बार फिर वैश्विक व्यापार जगत में चर्चा का विषय बन गई है। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप प्रशासन ने आयात शुल्क (टैरिफ) को हथियार बनाकर देशों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई हो। इससे पहले भी ट्रंप ने कई देशों पर भारी शुल्क लगाया था, लेकिन दबाव और राजनयिक बातचीत के चलते 90 दिनों के लिए अस्थायी रोक भी लगा दी थी।
हालांकि अब एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ नीति को दोहराते हुए 14 देशों पर आयात शुल्क लागू करने का ऐलान किया है। सोमवार को इस फैसले की औपचारिक जानकारी देते हुए ट्रंप ने सभी संबंधित देशों को लेटर के माध्यम से अवगत कराया है। ये 1 अगस्त से लागू होंगे।
इस नई घोषणा में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिका के एशिया में दो सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भी शामिल हैं। इन दोनों देशों से आयातित वस्तुओं पर 25 प्रतिशत तक का टैरिफ लगा दिया गया है।
फिलहाल भारत पर कोई नया टैरिफ लागू नहीं किया गया है, लेकिन ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि भारत के साथ एक व्यापार समझौता जल्द किया जा सकता है।
यह कदम ऐसे समय में आया है जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं पहले से ही अस्थिर हैं, और डॉलर वर्चस्व पर बहस के बीच अमेरिका एक बार फिर आक्रामक व्यापार नीति के जरिए वैश्विक बाजार पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है।

किन 14 देशों पर लगाया गया टैरिफ?
ट्रंप प्रशासन ने थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, लाओस, इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, सर्बिया और कंबोडिया जैसे 14 देशों पर 1 अगस्त 2025 से आयात टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है। इन सभी देशों को इस संबंध में आधिकारिक पत्र भेजा गया है।
टैरिफ की दरें किस पर कितनी?
ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू की गई आयात शुल्क की दरें देश के अनुसार अलग-अलग रखी गई हैं:
- थाईलैंड और कंबोडिया पर सबसे ज्यादा 36% टैरिफ लगाया गया है।
- बांग्लादेश और सर्बिया पर 35% शुल्क निर्धारित किया गया है।
- म्यांमार और लाओस को 40% टैरिफ के दायरे में रखा गया है।
- इंडोनेशिया पर 32% और
- दक्षिण अफ्रीका तथा बोस्निया पर 30% आयात शुल्क लगाया गया है।
- जबकि मलेशिया, कजाकिस्तान, जापान और दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ लागू किया गया है।
ट्रंप ने साथ ही चेतावनी दी यदि दक्षिण कोरिया या जापान अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाते हैं, तो अमेरिका न केवल अपने मौजूदा टैरिफ (25%) को बनाए रखेगा, बल्कि उसमें 5% या उससे अधिक की वृद्धि भी कर सकता है। उन्होंने साफ कहा, “अगर आप टैरिफ बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, तो जो भी दर आप बढ़ाएँगे, वह हमारे 25% में जोड़ दी जाएगी।“
आइए जानते है, टैरिफ क्या है?
टैरिफ (या आयात शुल्क) वह कर होता है जो सरकार किसी विदेशी देश से आयातित वस्तुओं पर लगाती है। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों की रक्षा करना होता है, ताकि सस्ते विदेशी सामान के मुकाबले स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल सके और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिले।
इतिहास की दृष्टि से, टैरिफ का प्रयोग प्राचीन काल से ही सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र करने के लिए किया जाता रहा है। वर्ष 1789 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने टैरिफ अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे। औपनिवेशिक युग में शक्तिशाली देश अपने उपनिवेशों पर भारी शुल्क लगाकर व्यापार को नियंत्रित करते थे—इस प्रणाली को मरकेंटिलिज़्म (Mercantilism) कहते हैं। लेकिन 20वीं सदी के अंत में जब वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिला, तब विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियमबद्ध किया जा सके।
टैरिफ क्यों लगाया जाता है?
सरकारें टैरिफ कई कारणों से लगाती हैं— जैसे स्थानीय उत्पादकों और लघु उद्योगों की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करना, और बेरोजगारी को रोकना। इसके अतिरिक्त, यह सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति का भी एक प्रमुख स्रोत होता है।
हालांकि, टैरिफ लगाने के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। इससे घरेलू कंपनियों में नवाचार की प्रवृत्ति घट सकती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघर्ष (Trade Rivalry) पैदा हो सकते हैं, और विकसित देश निर्धन या विकासशील देशों का आर्थिक रूप से शोषण कर सकते हैं। साथ ही, टैरिफ से आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे मुद्रास्फीति (Inflation) का खतरा भी होता है।
आम तौर पर टैरिफ का भुगतान आयात के समय किया जाता है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार सरकार आयात से पहले या बाद में भी शुल्क लगा सकती है। यह शुल्क आयातक कंपनी द्वारा आयात करने वाले देश की सरकार को अदा किया जाता है।
ट्रम्प ने जापान, दक्षिण कोरिया को टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में निर्माण का प्रस्ताव दिया –
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से बचने के लिए जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों को अमेरिका में विनिर्माण (manufacturing) के लिए प्रोत्साहित किया है। ट्रंप ने साफ कहा कि यदि इन देशों की कंपनियाँ अमेरिका में उत्पाद निर्माण करती हैं, तो उन पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। यह बयान उनके ‘मेक इन अमेरिका’ अभियान को बल देता है, जिसका उद्देश्य है आयात पर निर्भरता घटाना और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना।
ट्रम्प, जापान और दक्षिण कोरिया पर सख्त क्यों ?
गौरतलब है कि जापान और दक्षिण कोरिया अमेरिका के करीबी रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन ट्रेड डील अब तक नहीं हो पाई है। इसकी एक वजह यह भी है कि दोनों देशों में चुनाव होने वाले हैं, जिससे वे अभी कोई विवादास्पद व्यापार समझौता करने की स्थिति में नहीं हैं। दूसरी ओर, ट्रंप इन देशों के मुख्य उत्पादों जैसे कार, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी अलग से ज्यादा टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं, जिससे वार्ता और भी जटिल हो गई है।
भारत-अमेरिका टैरिफ वार्ता- जल्द ही आधिकारिक घोषणा होने की संभावना–:
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल को विश्व के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ (जैसे को तैसा शुल्क) लगाने की घोषणा की थी। हालांकि, इसे बाद में 90 दिनों के लिए टाल दिया गया, जिसकी डेडलाइन 9 जुलाई 2025 थी। अब इसे 1 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर तेज़ी से बातचीत जारी है।
अगर 1 अगस्त से पहले यह समझौता नहीं होता, तो भारत के ऊपर 26% का टैरिफ लागू हो सकता है, जिससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के अनुसार, वॉशिंगटन में दोनों देशों की टीमें लगातार बातचीत कर रही हैं, और जल्द ही इस डील की औपचारिक घोषणा हो सकती है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।
डील में मुख्य रुकावटें और मतभेद-
- कृषि और डेयरी सेक्टर पर असहमति: अमेरिका भारत में GM (Genetically Modified) फसलें और डेयरी प्रोडक्ट्स की बिक्री की मांग कर रहा है, जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। भारत का मानना है कि इससे खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और करोड़ों किसानों की आजीविका पर खतरा हो सकता है।
- टैरिफ नीति को लेकर विरोधाभास: भारत चाहता है कि अमेरिका पूरी तरह से 26% रेसिप्रोकल टैरिफ और 10% बेसलाइन टैरिफ हटाए, लेकिन अमेरिका केवल 10% टैरिफ बनाए रखने पर अड़ा है।
भारत की चिंताएं:
भारत की वार्ता टीम ने यह साफ कहा है कि खाद्य और डेयरी क्षेत्र बेहद संवेदनशील हैं — न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। जनस्वास्थ्य और किसान हितों को देखते हुए भारत ने GM फसलों और डेयरी बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने से इनकार किया है। भारत को डर है कि अमेरिकी मांगें मानने से घरेलू किसानों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को गहरी चोट पहुंच सकती है।
संभावित डील से भारत और अमेरिका दोनों को क्या लाभ?
यदि यह मिनी ट्रेड डील सफल हो जाती है, तो दोनों देशों को कई रणनीतिक लाभ हो सकते हैं:
- भारत के लिए संभावित लाभ: टेक्सटाइल, फार्मा और ज्वेलरी जैसे उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, इसके अतिरिक्त 26% टैरिफ हटने से भारतीय उत्पाद अमेरिका में सस्ते हो जाएंगे, जिससे निर्यात बढ़ेगा। और अनुमान है कि 2030 तक भारत-अमेरिका व्यापार 500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।
- अमेरिका के लिए संभावित लाभ: पेकान नट्स, ब्लूबेरी और ऑटोमोबाइल जैसे अमेरिकी उत्पादों को भारत में कम टैरिफ पर बेचने का अवसर मिलेगा, जिससे एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलेगी।
ब्रिक्स देशों को भी ट्रंप की चुनौती:
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स समूह को खुली चेतावनी दी है कि यदि वे अमेरिका विरोधी नीतियों या फैसलों का समर्थन करते हैं, तो उन पर 10% अतिरिक्त आयात शुल्क (Tariff) लगाया जाएगा। ट्रंप की यह धमकी ऐसे समय आई है जब ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता कम करने और एक साझा ब्रिक्स मुद्रा (BRICS Currency) की दिशा में काम कर रहे हैं। यह प्रयास अमेरिकी डॉलर के वैश्विक दबदबे को चुनौती देने वाला माना जा रहा है।
ब्रिक्स देशों की योजना है कि वे आपसी व्यापार में डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्राओं या संभावित ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल करें। अमेरिका इसे अपने आर्थिक वर्चस्व पर सीधी चुनौती के रूप में देखता है।