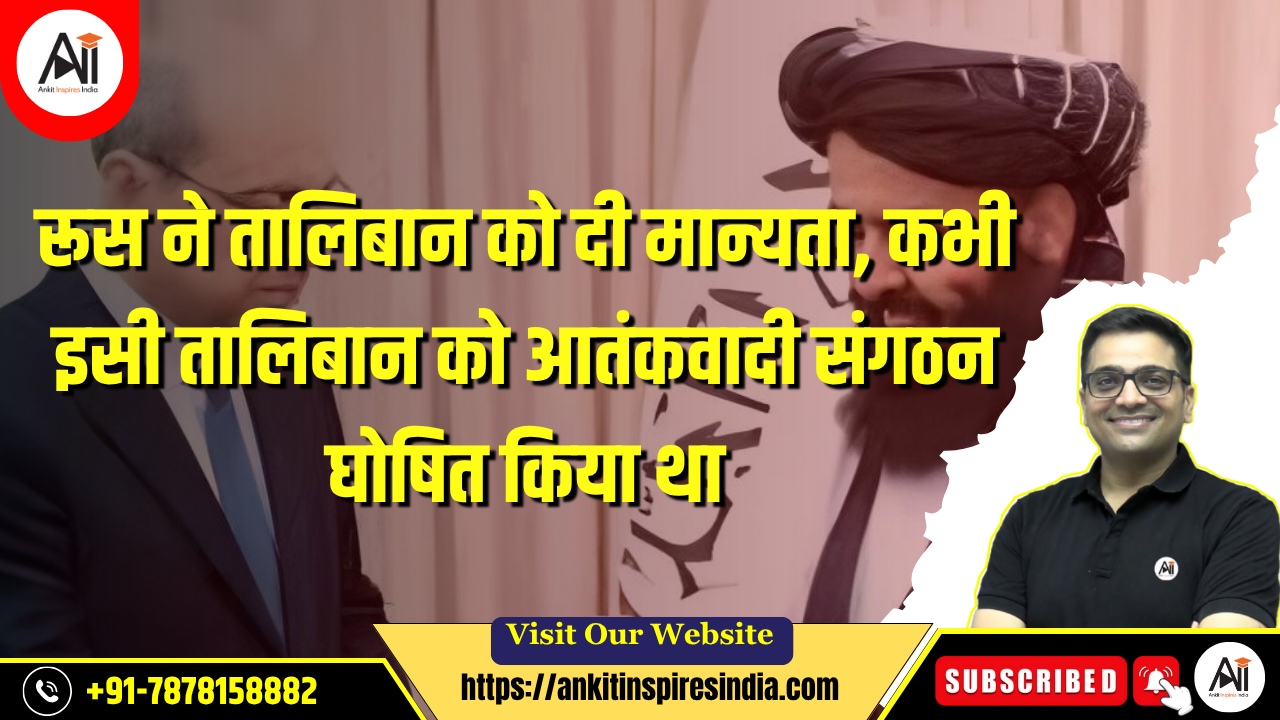रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दे दी है, जिससे वह दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने तालिबान शासन को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। यह फैसला अमेरिका की सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ने के चार साल बाद आया है, जब से तालिबान ने सत्ता अपने हाथ में ली थी।
अब तक तालिबानी सरकार को किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी थी — यहां तक कि पाकिस्तान ने भी नहीं, जिसे तालिबान का प्रमुख सहयोगी माना जाता था। ऐसे माहौल में रूस का यह कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संकेत माना जा रहा है।
रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान की सरकार को मान्यता देना हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा लाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा।”
अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने रूस के इस फैसले को “साहसिक कदम” बताया और उम्मीद जताई कि बाकी देश भी इससे प्रेरणा लेंगे।
यह घटनाक्रम न केवल अफगानिस्तान के लिए अहम है, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों में रूस की भूमिका को भी नया आकार देता है।

अफगानिस्तान का इतिहास: अंग्रेज़ों से लेकर रूस और अमेरिका तक का प्रभाव
अफगानिस्तान का इतिहास अस्थिरता, संघर्ष और विदेशी हस्तक्षेपों से भरा रहा है। पहले 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेज़ों ने इसे अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए इस्तेमाल किया और तीन एंग्लो-अफगान युद्धों के बाद भी अफगान जनता के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला बुझी नहीं। 1919 में अफगानिस्तान ने ब्रिटिश प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्रता की घोषणा की।
इसके बाद शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ (रूस) ने यहाँ सैन्य और राजनीतिक दखल दिया, तो फिर 2001 के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज की। इन हस्तक्षेपों ने अफगान समाज, राजनीति और सुरक्षा ढांचे को बार-बार बदल कर रख दिया।
आइए जानते हैं कि कैसे ब्रिटेन, रूस और अमेरिका ने अफगानिस्तान को अपने-अपने हितों के लिए प्रयोग किया और इसका क्या असर पड़ा।
अंग्रेजों का पहला हमला और अफगान जीत (1839–1842): 1839 में जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर पहला हमला किया। प्रारंभ में ब्रिटिश सेना को सफलता मिली, लेकिन दो साल के भीतर अफगानी सेनाओं ने उन्हें करारी हार दी। और अंग्रेजों को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा।
दूसरा एंग्लो-अफगान युद्ध और गंदमक संधि (1878–1880): लगभग 36 वर्षों बाद, 1878 में ब्रिटिश साम्राज्य ने अफगानिस्तान पर दोबारा आक्रमण किया। इस बार उन्हें विजय मिली और गंदमक नामक संधि हुई। सर लुईस कावानगरी और याकूब खान के बीच हुए इस समझौते को बाद में याकूब खान ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद पुनः युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने कंधार में जीत हासिल की और अब्दुल रहमान खान को सत्ता सौंप दी।
डूरंड रेखा का निर्माण (1893): ब्रिटिश इंडिया सरकार ने मॉर्टिमर डूरंड को 1893 में काबुल भेजा, जहाँ अफगानिस्तान के शासक अब्दुल रहमान खान से एक समझौता हुआ। 12 नवंबर 1893 को दोनों पक्षों ने पाराचिनार के पास नक्शे पर एक सीमा रेखा खींची, जिसे डूरंड लाइन कहा गया। इस रेखा ने खैबर पख्तूनख्वा, फ्रंटियर रीजन्स और फाटा को ब्रिटिश इंडिया में और नूरिस्तान एवं वखान को अफगानिस्तान में शामिल किया।
तीसरा एंग्लो-अफगान युद्ध और स्वतंत्रता (1919): 1919 में ब्रिटिश इंडिया ने अफगानिस्तान पर तीसरी बार हमला किया। इस युद्ध के अंत में रावलपिंडी समझौता हुआ जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य ने अफगानिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी और बदले में अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन को अंतरराष्ट्रीय सीमा माना।
भारत-पाक विभाजन और डूरंड लाइन विवाद (1947–1949): भारत के बंटवारे के बाद डूरंड लाइन पाकिस्तान की सीमा बन गई। पश्तून आबादी इस विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित हुई। 1949 में पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा अफगानी सीमा पर हमले के बाद अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन ने 1950 में हस्तक्षेप कर इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा घोषित किया, लेकिन विवाद समाप्त नहीं हुआ।
सरदार दाऊद खान की पहल और संबंधों में सुधार (1976)
1976 में अफगान शासक सरदार मोहम्मद दाऊद खान इस्लामाबाद आए और डूरंड लाइन को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार किया। इस पहल से दोनों देशों के संबंध सुधरे और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के विरुद्ध सहयोग करना शुरू किया।
सोवियत आक्रमण: मैत्री संधि के बहाने काबुल पर कब्ज़ा
24 दिसम्बर 1979 को सोवियत रूस ने 1978 की सोवियत-अफगान मैत्री संधि को बनाए रखने के बहाने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। आधी रात को काबुल में सोवियत सैन्य हवाई जहाजों का विशाल बेड़ा उतरा, जिसमें करीब 280 परिवहन विमान और 8,500 सैनिकों की तीन डिवीजन शामिल थीं। कुछ ही दिनों में ताजबर्ग पैलेस पर विशेष हमला करके काबुल पर नियंत्रण कर लिया गया। हालांकि हफीजुल्लाह अमीन के प्रति वफादार अफगान सैनिकों ने जबरदस्त प्रतिरोध किया।
27 दिसंबर को सोवियत समर्थक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान (PDPA) के निर्वासित नेता बबरक कर्मल को अफगानिस्तान का नया प्रमुख घोषित किया गया। इसी के साथ सोवियत जमीनी सेना ने उत्तर दिशा से अफगानिस्तान में प्रवेश कर लिया, और देश में उनकी सीधी सैन्य उपस्थिति की शुरुआत हुई।
काबुल जैसे शहरों में सफलता के बावजूद जब सोवियत सेना ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में पहुँची, तो उन्हें मुजाहिदीनों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने अफगान सीमा पर अपने लड़ाकों को तैनात किया और उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने अमेरिकी CIA सक्रिय हुई, सोवियत दबदबे को तोड़ने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ‘ऑपरेशन साइक्लोन’ नाम से एक गुप्त मिशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से मुजाहिदीनों को हथियार, धन और प्रशिक्षण देना शुरू किया। 1986 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इन्हें स्टिंगर मिसाइलें भी देना शुरू कर दीं, जिससे सोवियत सेनाओं को भारी नुकसान हुआ।
यह ऑपरेशन CIA के इतिहास का सबसे महंगा और बड़ा गुप्त मिशन था, और इसी के दौरान अफगानिस्तान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का ‘वार ज़ोन’ बन गया।
स्टिंगर मिसाइलों ने बदली युद्ध की दिशा
1987 में अमेरिका ने मुजाहिदीनों को कंधे से दागी जाने वाली स्टिंगर एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइलें देना शुरू किया। इससे मुजाहिदीन पहली बार नियमित रूप से सोवियत विमानों और हेलीकॉप्टरों को गिराने में सफल हुए। इस तकनीकी बढ़त ने युद्ध का संतुलन पूरी तरह पलट दिया।
सोवियत संघ का अफगानिस्तान से बाहर निकलने का निर्णय
सोवियत संघ के नए नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अफगानिस्तान से बाहर निकलने का निर्णय लिया। जीत की कोई संभावना न देख 1988 में वापसी की प्रक्रिया शुरू की गई, और आखिरकार 15 फरवरी 1989 को अंतिम सोवियत सैनिक ने अफगान धरती छोड़ी।
इस युद्ध में सोवियत संघ के 15,000 से अधिक सैनिक मारे गए। युद्ध के आर्थिक और जनसंपर्क प्रभावों से सोवियत संघ कभी उबर नहीं पाया, और यह 1991 में उसकी विघटन की एक बड़ी वजह बना। 1989 में सोवियत सेना की वापसी के बाद, अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार ढह गई और इस्लामी लड़ाकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इन्हीं मुजाहिदीनों से धीरे-धीरे ‘तालिबान’ नामक कट्टरपंथी संगठन उभरा, जिसकी स्थापना 1994 में मुल्ला उमर ने की।
इसलिए कहा जा सकता है कि अमेरिका ने तालिबान को सीधे तौर पर नहीं बनाया, लेकिन जिस मुजाहिदीन आंदोलन को उसने सोवियत विरोधी रणनीति के तहत खड़ा किया, उसी की कोख से तालिबान ने जन्म लिया। यानी तालिबान का उदय उस भू-राजनीतिक खेल का अप्रत्याशित परिणाम था, जिसे अमेरिका ने सोवियत संघ को रोकने के लिए शुरू किया था।
तालिबान का इतिहास: अफगानिस्तान की धरती पर फिर से कट्टर इस्लामी शासन का उदय
अफगानिस्तान की धरती दशकों से जंग और अशांति का केंद्र रही है, और इस त्रासदी के मूल में तालिबान नामक संगठन की अहम भूमिका रही है। 1990 के दशक में, जब सोवियत सेना अफगानिस्तान से पीछे हट रही थी, उसी समय उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय हुआ। यह संगठन मूलतः पश्तून छात्रों द्वारा स्थापित किया गया, जिन्होंने पाकिस्तान के मदरसों में कट्टर इस्लामी शिक्षा प्राप्त की थी। ‘तालिबान’ शब्द का अर्थ होता है – ‘छात्र’। इन्हीं छात्रों में से एक था पश्तून समुदाय का सदस्य मुल्ला मोहम्मद उमर, जिसने बाद में तालिबान की स्थापना की। वर्ष 1994 में कंधार को संगठन का केंद्र बनाकर शुरू हुए इस आंदोलन ने धीरे-धीरे पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया।
तालिबान का पहला शासन और कट्टर इस्लामी कानूनों की शुरुआत:
तालिबान ने 1995 में हेरात और फिर 1996 में कंधार पर कब्जा करने के बाद राजधानी काबुल पर अधिकार कर लिया। तत्कालीन राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटा दिया गया, जो स्वयं एक समय में मुजाहिदीन के अग्रणी नेता थे। वर्ष 1998 तक तालिबान अफगानिस्तान के लगभग 90% हिस्से पर शासन कर रहा था। शुरुआत में लोगों ने तालिबान का स्वागत किया, क्योंकि वे गृहयुद्ध और अराजकता से थक चुके थे। लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि तालिबान केवल सत्ता स्थापित करने नहीं आया है, बल्कि एक कट्टर इस्लामी शासन को लागू करना उसकी मुख्य मंशा थी। इसके बाद देश में सार्वजनिक फाँसी, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर रोक, संगीत और टीवी पर प्रतिबंध, लड़कियों के स्कूल जाने पर मनाही और महिलाओं को अनिवार्य रूप से बुर्का पहनने जैसे नियम लागू किए गए।
2003: रूस द्वारा तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया
साल 2003 में रूस की सर्वोच्च अदालत ने तालिबान को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इस निर्णय के बाद तालिबान को रूस में न केवल गैरकानूनी माना गया, बल्कि उससे किसी भी प्रकार के संपर्क को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया। यह कदम रूस ने अफगानिस्तान और मध्य एशिया में आतंकवाद फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए उठाया था।
तालिबान का पतन: 9/11 के बाद अमेरिका का हस्तक्षेप
तालिबान दुनिया के सामने उस समय खतरनाक रूप में आया जब अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ। हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन था, जिसे तालिबान ने अफगानिस्तान में पनाह दी हुई थी। अमेरिका ने ओसामा को सौंपने की मांग की, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप करते हुए अक्टूबर 2001 में तालिबान की सत्ता को समाप्त कर दिया। मुल्ला उमर और उसके अन्य सहयोगी पाकिस्तान भाग गए और वहीं से फिर अपनी वापसी की योजना बनाने लगे। अमेरिका के नेतृत्व में अफगानिस्तान में एक नई लोकतांत्रिक सरकार बनी, लेकिन तालिबान ने हमले जारी रखे, और देश में अस्थिरता बनी रही।
दूसरे दौर की वापसी और अमेरिका का सैनिक हटाव:
2004 से लेकर 2021 तक, तालिबान ने छिटपुट हमलों और आत्मघाती हमलों के ज़रिए अपनी ताकत बढ़ाई। अमेरिका ने अफगानिस्तान में कुल 822 अरब डॉलर खर्च किए, और इस संघर्ष में उसके 2300 से अधिक सैनिक मारे गए, जबकि 20,000 से अधिक घायल हुए। 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ‘अंतहीन युद्धों’ से थके अमेरिका को सैनिक वापस बुलाने का वादा किया। उन्होंने मई 2021 तक वापसी की समयसीमा तय की। बाद में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस समयसीमा को बढ़ाया और सैनिकों की वापसी शुरू की। इसी बीच, तालिबान ने 2018 में अमेरिका के साथ बातचीत शुरू की और फरवरी 2020 में दोहा (कतर) में समझौता हुआ। इसके अनुसार अमेरिका सैनिकों को वापस बुलाने और तालिबान विदेशी सेनाओं पर हमले रोकने पर सहमत हुए। तालिबान ने यह भी आश्वासन दिया कि वह अल-कायदा और अन्य आतंकी संगठनों को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देगा।
15 अगस्त 2021: तालिबान की सत्ता में वापसी और नई चिंता
इस समझौते के बाद तालिबान ने हमले और तेज़ कर दिए और आखिरकार 15 अगस्त 2021 को काबुल पर कब्जा कर लिया। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण स्थापित हो गया। लेकिन इस बार भी उसके शासन की शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। महिलाओं के अधिकार फिर से छीन लिए गए, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं की पढ़ाई पर रोक लगा दी गई, मीडिया की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया और विरोधियों पर अत्याचार शुरू कर दिए गए।
अब अंतरराष्ट्रीय मान्यता की जद्दोजहद
तालिबान की सत्ता को अभी तक अमेरिका, भारत समेत अधिकांश देशों ने मान्यता नहीं दी है। तालिबान का दावा है कि उसने सरकार के लिए आवश्यक सभी शर्तें पूरी कर ली हैं – जैसे सीमित क्षेत्र, स्थायी जनसंख्या, सरकार और विदेशी संबंध स्थापित करने की क्षमता – जो कि 1933 की मोंटेवीडियो संधि के तहत मान्यता के लिए आवश्यक हैं। लेकिन दुनिया इसे मान्यता देने से कतरा रही है, खासकर अमेरिका के दबाव के कारण। वहीं, पाकिस्तान पर आरोप है कि उसने तालिबान को शिक्षा, प्रशिक्षण और पनाह दी, और 2021 की लड़ाई में भी पूरी मदद की। इसी वजह से अफगान सरकार द्वारा पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी।
रूस ने क्यों दी तालिबान को मान्यता?
रूस द्वारा तालिबान को मान्यता देने के पीछे कई रणनीतिक और भू-राजनीतिक कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण यह है कि रूस नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की भूमि का उपयोग ISIS-K, अल-कायदा या अन्य चरमपंथी संगठनों द्वारा रूस या मध्य एशियाई देशों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाए। तालिबान के साथ औपचारिक संबंध बनाने से रूस को अफगानिस्तान की सत्ता पर सीधा प्रभाव बनाए रखने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा, रूस को मध्य एशिया में स्थिरता की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ की सुरक्षा उसकी दक्षिणी सीमाओं से सीधी तौर पर जुड़ी हुई है। रूस अफगानिस्तान में एक ऐसी सत्ता चाहता है जो किसी सत्ता-शून्यता (power vacuum) की स्थिति में आतंकवाद को पनपने न दे।
इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अमेरिका लगातार मध्य पूर्व (Middle East) में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस अब अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद मध्य पूर्व में अपनी रणनीतिक पकड़ दोबारा मजबूत करना चाहता है। तालिबान को मान्यता देकर रूस न केवल अफगानिस्तान में स्थिरता की भूमिका निभा रहा है, बल्कि वह मध्य एशिया और मध्य पूर्व में अपने प्रभाव क्षेत्र को पुनः स्थापित करने की दिशा में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
कौन से देश अब भी तालिबान को आतंकी संगठन मानते हैं?
भले ही रूस ने तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता दे दी है, लेकिन कई देश अब भी इसे आतंकी संगठन या अवैध सत्ता के रूप में ही देखते हैं। भारत ने अब तक तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है और इसे सतर्क निगाहों से देखता है. पाकिस्तान के साथ हुए विवाद के बाद दोनों देशों में नजदीकियां देखने को मिली थी, वहीं, अमेरिका और यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों ने भी तालिबान को अब तक मान्यता नहीं दी है। वे महिला अधिकार, लोकतांत्रिक शासन और मानवाधिकारों की बहाली की शर्त पर ही आगे किसी तरह की मान्यता देने की बात करते हैं।
तालिबान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति और आगे की राह
आज तालिबान खुद को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मान्यता की कमी, आर्थिक संकट, मानवाधिकारों का हनन और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उसकी राह कठिन बना दी है। अफगानिस्तान में लाखों लोग मानवीय संकट से जूझ रहे हैं, भूख, बेरोजगारी और असुरक्षा चरम पर है। दुनिया की निगाहें एक बार फिर अफगानिस्तान पर हैं, और सवाल अब भी वही है – क्या तालिबान बदला है या फिर इतिहास दोहराया जा रहा है?